BBC विशेष
लिंक
एहसासों को बेहतर बयां करतीं स्थानीय बोलियां
 BBC/GETTY IMAGES
BBC/GETTY IMAGES
हर ज़बान अपने आप में मुकम्मल है. ख्याल और जज़्बात के इज़हार के लिए पर्याप्त शब्द हैं. फिर भी बहुत से ऐसे एहसास हैं, जिन्हें बयां करने के लिए हमारे पास लफ़्ज़ कम पड़ जाते हैं.
अगर ज़ायक़े की बात करें तो मोटे तौर पर हम खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा यही बताते हैं. लेकिन, कई बार ज़ायक़े बताने के लिए माक़ूल अल्फ़ाज़ नहीं मिलते. हो सकता है हमारी ज़बान में ऐसे शब्दों की क़िल्लत हो. लेकिन, अन्य भाषाओं में उनके लिए बेहतर शब्द हो सकते हैं. दरअसल रंग, ख़ुशबू, ज़ायक़ा आदि बयान करने के लिए हम जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी संस्कृति और समुदाय की अक्कासी होती है.
माना जाता है कि अंग्रेज़ी ज़बान का शब्दकोश सबसे ज़्यादा समृद्ध है. अंग्रेज़ी में जितने विशेषण और क्रिया शब्द हैं, उतने किसी और भाषा में नहीं हैं. लेकिन, हालिया रिसर्च से साबित होता है कि दुनिया देखने और आस-पास का माहौल महसूस करके उसे बयान करने के लिए जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, उससे हमारी पूरी संस्कृति ज़ाहिर होती है.
ये रिसर्च यूरोप, उत्तरी-दक्षिण अमरीका, एशिया, अफ़्रीक़ा, और ऑस्ट्रेलिया की 20 भाषाओं पर की गई है. रिसर्च में शामिल प्रतिभागियों से मीठे पानी का ज़ायक़ा बताने, ख़ुशबू वाला पेपर सूंघ कर उसकी ख़ुशबू बताने, और रंगीन पेपर देखकर उसका रंग बताने को कहा गया. किसी ने सटीक रंग बताया तो कोई ख़ुशबू के लिए उचित शब्द इस्तेमाल कर पाया. वहीं, कोई चीनी वाले पानी के लिए सही शब्द बता सका.
लेकिन, किसी एक ने भी तीनों के लिए सटीक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया.
इस रिसर्च की अगुवा आसिफ़ा माजिद ने मलय प्रायद्वीप की घुमंतू जाति जहाए पर भी रिसर्च की. उन्होंने पाया कि इस समुदाय के लोग चूंकि जंगलों में रहते हैं, लिहाज़ा वो हरेक तरह की ख़ुशबू को बेहतर जानते हैं. इसीलिए उनकी ज़बान में अलग-अलग ख़ुशबू के लिए कई तरह के शब्द हैं. इस मामले में इनकी ज़बान अंग्रेज़ी भाषा से भी ज़्यादा समृद्ध है. जबकि, रंग और ज़ायक़ों के लिए इनके पास चंद ही शब्द हैं.
- 'डेड' झील कराकुल जहां नाव तक नहीं चल सकती
- जापान के आधुनिक संतों की दुर्दशा
- हाथी को कैसे बचा सकती है टेक्नॉलॉजी
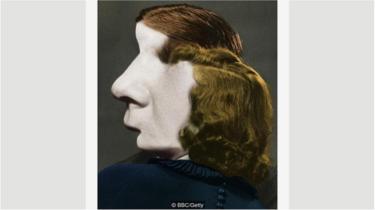 BBC/GETTY
BBC/GETTYरंग और ज़ायकों को बेहतर बताती स्थानीय बोलियां
ऑस्ट्रेलिया में आम तौर से अंग्रेज़ी बोली जाती है. लेकिन चंद लोग उम्पिला भाषा बोलते हैं. रिसर्च में इन्हें भी शामिल किया गया. रिसर्च में कुल 313 लोग शामिल हुए थे और सभी को अलग-अलग ग्रुप में बांट कर इनका कोडेबिलिटी टेस्ट किया गया.
यानि अगर किसी एक चीज़ के लिए एक समूह के कमोबेश सभी सदस्यों ने एक ही शब्द इस्तेमाल किया तो माना गया कि उनका कोडेबिलिटी स्तर ऊंचा है. और जिस ग्रुप के प्रतिभागियों ने किसी चीज़ के लिए अलग-अलग लफ़्ज़ इस्तेमाल किए उसका कोडेबिलिटी स्तर निम्न माना गया. पाया गया कि अंग्रेज़ी बोलने वालों में रंग और आकार को लेकर लगभग सभी में समानता थी.
वहीं, फ़ारसी ज़बान में ज़ायक़ों के लिए बहुत तरह के शब्द हैं और सभी की हर शब्द पर सहमति है. मसलन कड़वे ज़ायक़े के लिए फ़ारसी बोलने वाले तल्ख़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अंग्रेज़ी में इस ज़ायक़े के लिए बहुत से शब्द हैं. और लोग एक ही ज़ायक़े के लिए कई तरह के लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं. लोगों के ज़हन में एक ही ज़ायक़ा बयान करने के लिए दुविधा बनी रहती है.
रिसर्च में पाया गया है कि जिन संस्कृतियों में खाने का चलन ज़्यादा है और बहुत तरह के पकवान पकते हैं उनकी भाषा में ज़ायक़ा बताने के लिए सटीक शब्दों का इस्तेमाल होता है. इसी तरह जो समुदाय जंगलों में रहते हैं या प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, वो रंगों की बहुत ज़्यादा पहचान नहीं कर पाते. जबकि हर तरह की ख़ुशबू पहचान लेते हैं.
- कार बनाने आए थे, अब चेन्नई को नये व्यंजन परोस रहे हैं
- हर्बल चाय या फलाहार का हमारी आंतों पर क्या असर
- जानवर काटने को 'ना' पर गोश्त को 'हाँ'
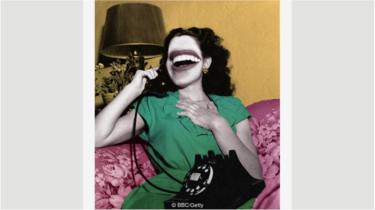 BBC/GETTY
BBC/GETTY
इशारों की ज़बान इस्तेमाल करने वालों में भी इस तरह की विविधता देखने को मिलती है. मिसाल के लिए बाली के काटा कोलोक गांव में क़रीब 1200 लोग इशारों की भाषा बोलते और समझते हैं. ये भी ऑस्ट्रेलिया के घुमंतू समुदाय उम्पिला के लोगों की तरह कई रंगों के नाम नहीं जानते. जबकि अमरीका या ब्रिटेन में इशारों की ज़बान बोलने वाले बहुत से रंगों के नाम जानते हैं.
इसी तरह जो लोग एक ही तरह के घरों में रहते हैं, उनकी ज़बान में कई आकारों के लिए शब्द नहीं हैं. रिसर्च में संगीत से संबंध रखने वाले बहुत से प्रतिभागी शामिल थे. इनकी भाषा में कई तरह की आवाज़ों के लिए कई शब्द थे. इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग संगीत की दुनिया में रहते हैं वो संवाद के लिए अपनी ही शब्दावली तैयार कर लेते हैं जिसमें अलग-अलग आवाज़ों के लिए बहुत से शब्द हैं.
दरअसल, भाषा का मतलब ही है समानता. जब तक संवाद में शामिल लोग एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, संवाद संभव नहीं होगा. इस मामले में अभी तक अंग्रेजी ज़बान ही सबसे ज़्यादा समृद्ध है. शायद इसलिए भी कि ये ज़बान दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है. अंग्रेज़ी जहां पहुंची वहां के स्थानीय शब्द इसने अपना लिए. अच्छा तो ये होगा कि हम अपनी ज़बान में नए-नए शब्द शामिल करके उसे और ज़्यादा दमदार बनाएं


No comments:
Post a Comment